प्रशन 1 से 19 तक के प्रश्नों के उत्तर के
लिए क्लिक करे
प्रशन 20:—क्षेत्रीय दलों के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए।
या :—क्षेत्रीय दलों के उदय पर एक टिप्पणी लिखें।
उत्तर:—भारत
में क्षेत्रीय दलों का अति आवश्यक है। क्षेत्रीय दलों के होने के निम्न दो कारण
हैं।—
(1) भारत
एक विशाल देश है, जिसमें विभिन्न भाषाओं, धर्मो तथा
जातियों के लोग रहते हैं। अनेक क्षेत्रीय दलों का निर्माण जाति, धर्म
एवं भाषा के आधार पर हुआ है।
(2) भारत
एक विस्तृत देश है जिसकी भौगोलिक बनावट में विभिन्न ताई पाई जाती है। विभिन्न
क्षेत्रों की अपनी समस्याएं तथा आवश्यकताएं हैं। इनकी पूर्ति के लिए विभिन्न
क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है।
(3) भारतीय
राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय राजनीतिक दालों का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा
है। 30 सितंबर, 2000 तक चुनाव आयोग के पास 682
राजनीतिक राजनीतिक दल पंजीकृत थे। 29 मार्च,2004 को
चुनाव आयोग ने 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल
के रूप में तथा 56 राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय दल के रूप में
मान्यता प्रदान की। सितंबर अक्टूबर, 1999 में 13
वीं लोकसभा के चुनाव से पहले और बाद में भी क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत
महत्वपूर्ण रही।भारतीय जनता पार्टी ने 24 दलों के साथ
मिलकर एक महान गठबंधन बनाया जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नाम दिया गया।
लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के बाद इस गठबंधन के अधिकांश सदस्यों को सरकार में
भी सम्मिलित किया गया। 2004 के 14 वें लोकसभा
चुनाव में भी किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। जिसके कारण कांग्रेश के नेतृत्व मैं
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का निर्माण किया गया , जिसमें कई
क्षेत्रीय दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्र में सरकार स्थापित करने के
अलावा अनेकों राज्यों में भिन्न-भिन्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने सरकार ने बनाई
है।
*क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण:—
दालों के उदय के कारण निम्नलिखित है—
(1) राष्ट्रीय
छवी के नेताओं का अभाव है जिसके कारण स्थानीय सतर के चतुर क्षेत्रीय नेताओं ने
अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने हेतु जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद
जैसे तत्वों का सहारा लिया।
(2) देश
में चुनाव संबंधी ऐसा कोई कानून नहीं है, जो न्यूनतम सीमा
के नीचे मत पाने वाले दलों के प्रतिनिधित्व को अमान्य कर सके।
(3) सभी
दलों ने अपने विचारधारा को त्यागकर पूर्णरूप से अवसरवादी राजनीति का सहारा लिया है, जिससे
ऐसी अवांछनीय स्थिति पैदा हुई है।
प्रशन 21:—गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं?
गठबंधन सरकार के अवगुणों को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:— वह
राजनीति जिससे चुनाव के पहले अथवा बाद में आवश्यकतानुसार दलों में सरकार गठन या
किसी अन्य मामले पर आपसी सहमति बन जाए और वे सामान्यतः स्वीकृत न्यूनतम साझा
कार्यक्रम के अनुसार देश में राजनीति करें (विरोधी दल के रूप में या सत्ताधारी गुट
के रूप में) तो ऐसी राजनीति को गठबंधन की राजनीति कहते हैं।
*अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक
गठबंधन) अथवा डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व मैं गठित प्रगतिशील (संप्रग) गठबंधन
की राजनीति को स्पष्ट करते हैं। 1989 के बाद भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी
परिवर्तन आया। कांग्रेस दिनों-दिन कमजोर होती चली गई। दूसरी ओर भाजपा की
लोकप्रियता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई ।
* गठबंधन सरकार के कुछ अवगुण होते हैं, जो इस प्रकार हैं—
(1) गठबंधन
सरकार आपसी खींचा-तानी का शिकार होती है।
(2) इस
प्रकार की सरकार में अनेक दल शामिल होते हैं, जिनके कारण
पार्टी द्वारा घोषित कार्यक्रमों को जनता के बीच लागू कर पाना कठिन होता है।
(3) समझौता
करना गठबंधन सरकार की विवशता है, क्योंकि अन्य दलों की बैसाखी के सहारे टिकी
अल्पमत सरकार को किसी भी क्षण गिरने का खतरा बना रहता है।
(4) इसमें
विभिन्न हितों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए जनता के प्रति पूर्ण
जवाबदेही और सामूहिक नेतृत्व की भावना का अभाव रहता है।
(5) क्षेत्रियता
की भावना गठबंधन में ज्यादा पनपति है। जो केंद्र सरकार के माध्यम से क्षेत्रीय
हितों की पूर्ति करते हैं।
प्रशन 22:— भारत की नई आर्थिक नीति के प्रमुख लक्षणों की विवेचना करें।
उत्तर:—कोई
राज्य दुनिया कट कर दिया अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के प्रभाव से बचकर नहीं रह सकता।
जब 1991 में नरसिंह राव ने अपनी सरकार बनाई तो उन्हें अपने वित्त मंत्री
मनमोहन सिंह के परामर्श को मानकर नहीं आर्थिक नीति अपनानी पड़ी। इसके मुख्य
लक्षणों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—
(1) नेहरू
इंग्लिश समाजवाद से प्रभावित थे, अतः उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के
अधिकाधिक नियंत्रण को अनिवार्य समझा। उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को सराहा।
पंचवर्षीय योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाने पर जोर दिया गया। पहले जमीन
दारी का उन्मूलन और फिर जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया इंदिरा गांधी
ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। लेकिन अब मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक चित्र की जगह
निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की नीति अपनाई। लाइसेंस, परमिट
व कोटा जैसी हटां या कम कर दी गयी। धीरे-धीरे बाजार को खोल दिया गया।
(2) सार्वजनिक
क्षेत्र के उद्योगों को घाटे से बचाने के लिए विनिवेशीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई।
सार्वजनिक उदम में निजी हिस्सेदारों का अनुपात बढ़ा दिया गया।
(3) निजी
संस्थाओं को अपने उद्योग की अनुमति दी गई तथा एकाधिकार को रोकने वाले उद्योगों के
अधिकार क्षेत्र या उसके हस्तक्षेप में कमी की गई।
(4) सरकार
ने विदेशी पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन दीया। उन्हें किसी महत्वपूर्ण उद्योग में 51 /निवेश
तक करने की अनुमति दी गई।
(5) सार्वजनिक
उद्दमों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक स्वायत्तता दी गई तथा उनके
प्रबंध मंडलों को अधिक व्यवसायिक बना दिया गया।
(6) विदेशी
तकनीकी व विदेशी विशेषज्ञों के आगमन को छूट मिल गई।
(7) बीमा
या दुर्बल सार्वजनिक उद्यमों को औद्योगिक व वित्तय पुनः निर्माण के हवाले किया गया, ताकि
उनके पुनः जीवित करने की योजनाएं बनाई जा सके। इन
सभी सुधारों के पीछे यह प्रयास है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अविलम्ब सुधार करके
उसे विश्व में चल रही प्रतियोगिता के समकक्ष बनाया जाए। इसके तीन प्रमुख लक्षण है—उदारीकरण, निजीकरण
तथा वैश्वीकरण।
प्रशन 23:—आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया ने अर्थव्यवस्था पर क्या प्रतिकूल प्रभाव
डाले हैं संक्षेप में बताएं।
उत्तर:—आर्थिक
सुधारों की प्रक्रिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था मैं निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव डाले
हैं—
(1) कृषि
क्षेत्र में सुधार:—आर्थिक सुधारों
के अंतर्गत भारत सरकार ने खाद्य सब्सिडी को कम किया है, जबकि
न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। इनके सामूहिक प्रभाव से अनाज की कीमतों
में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में, सार्वजनिक
निवेश मैं विशेषकर आधारिक संरचना में काफी आई है।
(2) उद्दोग
क्षेत्र में सुधार:—आर्थिक सुधारों
की प्रक्रिया ने देश के उद्योगों को अत्यधिक आघात पहुंचाया है। बहुराष्ट्रीय
कंपनियां तो भारतीय बाजार को धीरे धीरे हड़प नहीं है, जबकि
भारत अभी भी विकसित राष्ट्रों को निर्यात कर पाने में विफल रहा है।
(3) विनिवेश:—अपनी
विनिवेश नीति के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को कम दामों पर निजी
क्षेत्रों की कंपनियों को बेचा जा रहा है। इस प्रक्रिया सेब सरकार को बहुत नुकसान
उठाना पड़ रहा है।
(4) व्यापार:—भारत
विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश है। इसने संगठन के नियमों के अनुसार अपनी
आयात-निर्यात नीति को उदार बना दिया है। आयातों पर लगे सभी मात्रात्मक नियंत्रण
हटा लिए गए हैं।
(5) बहुराष्ट्रीय
कंपनियों का आधिपत्य:—बहुराष्ट्रीय
कंपनियां अब धीरे-धीरे भारतीय बाजार पर कब्जा करती जा रही है और परिणामस्वरूप इनके
लाभों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।
प्रशन 24:—शीत युद्ध का अर्थ, प्रकृति एवं कारणों का वर्णन करें।
उत्तर:—द्वितीय
विश्व युद्ध की संपत्ति के बाद विश्व राजनीति में दो धुव्र बन गए। एक अमेरिका के
नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का पश्चिमी गुट रहा तो दूसरा सोवियत संघ के नृत्य में
पूर्वी देशों का समय वादी गुट। इन दोनों गुटों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई तथा दोनों ही गुटएक
दूसरे को समाप्त करने की खुली इच्छा का भी परिचय देने लगे। ऐसा लगने लगा कि शीघ्र
ही विश्व को तीसरे विश्वयुद्ध का सामना करना पड़ेगा।
यहां यह उल्लेखनीय है कि दोनों ही गुट संघर्ष की स्थिति तक पहुंचना
चाहते थे, भावनात्मक रूप से जितना एक-दूसरे के विरोधी थे, उतना
ही वे समकालीन शामली पृष्ठभूमि के कारण वास्तविक या प्रत्यक्ष युद्ध से बचना चाहते
थे। दोनों ही गुट विश्व युद्ध की विभीषिका को समझते थे और परमाणु शक्ति संपन्न
होने के कारण यह भी समझते थे कि युद्ध में परमाणु शास्त्रों के उपयोग के कारण
निश्चित रूप से विश्व सभ्यता नष्ट हो जाएगी।
शीत युद्ध का अर्थ वास्तविक या प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है, बल्कि
युद्ध की पृष्ठभूमि है। युद्ध का उन्माद है, इसमें युद्ध की
भाषाएं बोली जाती है, किंतु सरहदों पर गोली नहीं चलती है। शीत युद्ध
में प्रस्पर विरोधी गुटों द्वारा सामरिक अस्त्रों का विकास किया जाता है—उसके
निर्माण पर काफी खर्च किए जाते हैं, समर्थकों की
संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। एक दूसरे की नीतियों एवं कार्यक्रमों की
आलोचना की जाती है।
** शीत
युद्ध के कारण:-- शीत युद्ध के कारण निम्नलिखित बतलाए जा सकते
हैं----
1. द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ तथा
अमेरिका एवं ब्रिटेन के बीच वैचारिक दूरी बढ़ती गई। माल्टासम्मेलन की भावना के
निरादर का आरोप सोवियत संघ पर लगाया गया।
2. जर्मनी का बंटवारा दोनों गुटों के द्वारा कर
दिया गया। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत नियंत्रण स्थापित हो गया।
3. ईरान में सोवियत संघ की सेनाओं ने जमावड़ा बना
रखा था, जिसका विरोध ब्रिटेन करता था।
4. दोनों ही गुट परस्पर विरोधी प्रचार करते थे
जिससे अविश्वास, कलह, घृणा की स्थिति बनती थी।
5. परस्पर अविश्वास का ही परिणाम था कि सूरक्षा
परिषद् मैं इन गुटों के अग्रणी देशों को निषेध अधिकार दिया गया। वे अपने
वर्चस्वकारी स्थिति को बनाए रखना चाहते थे।
6. अमेरिका पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के
विस्तार वादी नीति का विरोध करता था। इस प्रकार शीतयुद्ध विभिन्न कारणों से
अस्तित्व में आया। किंतु समय के साथ द्विधु्वीयता की स्थिति समाप्त हुई। 1990 तक
सोवियत संघ का पतन हुआ। साम्यवादी जगत विघटीत हुई और इस प्रकार द्विधुवीय विश्व
राजनीति तथा शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम यह हुआ
कि अमेरिका वर्चस्व के अधीन विश्व एकध्रुवीय व्यवस्था की ओर आगे बढ़ा
प्रशन 25:—विश्व राजनीति में शीत युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें।
उत्तर:—शीत
युद्ध का तात्पर्य दो देशों की यादों के मध्य तनाव व संघर्ष की ऐसी स्थिति है
जिसमें सैनिक संघर्ष तो नहीं होता लेकिन अन्य साधनों से दोनों पक्ष एक दूसरे पर
आरोप-प्रत्यारोप व आपसी तनाव व अविश्वास की स्थिति में सलंग्नहोते हैं। द्वितीय
विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आधार पर विश दो विरोधी गुटों में बट गया एक पूंजीवादी
गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका के हाथ में था, दूसरा समय वादी
गुट जिसका नेतृत्व सोवियत संघ के हाथ में था। द्वितीय विश्व युद्ध से 1991 तक
का काल शीत युद्ध का काल कहा जाता है। 1991 में सोवियत संघ
के विघटन के उपरांत एक गुट का बिखराव हो गया तथा शीत युद्ध का अंत हुआ। शीत युद्ध
का अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर निम्न प्रभाव हुआ—
1. जिसका
दो गुटों में ध्रुवीकरण:—शीत
युद्ध के कारण विश्व के राष्ट्रों का दो गुटों में तिव्र ध्रुवीकरण। प्रत्येक गुट
ने अन्य देशों को अपने प्रभाव में लेने के लिए विभिन्न प्रकार के उचित व अनुचित
तरीके अपनाएं।
2. राज्यों
के मध्य अविश्वास व घृणा का विकास:—शीत
युद्ध में राजयो के मध्य घृणा व अविश्वास को जन्म दिया जिसमें विभिन्न मुद्दों पर
अंतराष्ट्रीय सहयोग की भावना क्षीण हो गई।
3. प्रत्येक
घुटने अपना प्रभाव बढ़ाने व के भय से सैनिक गठबंधनो को बढ़ावा दिया। पूंजीवादी देश
का प्रमुख सैनिक गठबंधन ‘नाटो’ था तथा समय वादी
देशों का सैनिक गठबंधन ‘वारसा संधि’ के रूप में
सामने आया।
4. शास्त्रीय
करण व आणविक शास्त्रों के विकास की होड़:—शीत
युद्ध ने शास्त्रों की दौड़ को बढ़ावा दिया । आणविक शास्त्रों का भी तेजी से विकास
हुआ तथा नि: शास्त्रीय करण के प्रयासों को असफलता हाथ लगी।
5. अंतराष्ट्रीय
संस्थाओं के महत्व में कमी:—शीत
युद्ध ने अंतराष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय कानून के
महत्व को कम किया। यह संगठन शीत युद्ध के अखाड़े बन गए थे।
6. अंतराष्ट्रीय
समस्याओं का समाधान:—अंतराष्ट्रीय
विकास के लिए शांति तथा सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन शीत युद्ध के कारण
अंतराष्ट्रीय विकास तो दूर अनेक वैशिवक समस्याओं का समाधान भी राजनीति का शिकार हो
गया।
ये भी पढ़े ...
Class 12th Political Science :- Click Here
Class 12th History :- Click Here


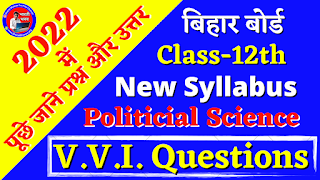
Hello My Dear, ये पोस्ट आपको कैसा लगा कृपया अवश्य बताइए और साथ में आपको क्या चाहिए वो बताइए ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ धन्यवाद |