प्रशन 1 से 12 तक के उत्तर के लिए क्लिक करे
उत्तर:-- Click Here
प्रशन 13:-- कश्मीर समस्या पर एक निबंध लिखें।
उत्तर:--
1947 में जब ब्रिटिश
भारत को भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किया गया तब महाराजा हरी सिंह कश्मीर तथा
जम्मू पर शासन कर रहे थे।
कश्मीर के पश्चिमी भाग में मुसलमानों ने महाराज के विरुद्ध बगावत की।
आक्रमण से सावधान होकर हरी सी सिंह ने
भारत से सैनिक सहायता की मांग की परंतु भारत ने तब तक मदद करने से इंकार कर दिया जब तक महाराज सम्मिलन के
दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं कर देता।इस
समझौते पर 27 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए। भारतीय सेना को तुरंत जम्मू
कश्मीर भेजा गया।भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में भी ले गया और पाकिस्तान पर
आक्रमण करने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र ने एक जनवरी 1949 को
युद्ध विराम लागू करवाया। पाकिस्तान द्वारा अधिगृहित कश्मीर को खाली कराने के लिए
भारत के आग्रह के बावजूद पाकिस्तान ने इसे खाली नहीं किया। जम्मू और कश्मीर की
जनता द्वारा निर्वाचित संविधान ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर भारत का
अभिन्न अंग है।
प्रशन 14:— भारत की विदेश नीति का विवेचन कीजिए।
उत्तर:
—साधारण
शब्दों में विदेश नीति से तात्पर्य उस नीति से है जो एक राज्य द्वारा दूसरे
राज्यों के प्रति अपनाई जाती है। वर्तमान युग में कोई भी स्वतंत्र देश संसार के
अन्य देशों से अलग नहीं रह सकता। उसे राजनीतिक ‚आर्थिक और
सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस
संबंधों को स्थापित करने के लिए वह जिन नीतियों का प्रयोग करता है उन नीतियों को
उस राज्य की विदेश नीति कहते हैं।
* भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं या
सिद्धांत या उद्देश्य
(1) गुट
निरपेक्षता :— दूसरे
विषय युद्ध के पश्चात विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। इसमें से एक पश्चिम
देशों का गुट था और दूसरा साम्यवादी देशों का। दोनों महाशक्तियों ने भारत को अपने
पीछे लगाने के काफी प्रयास किए , परंतु भारत ने दोनों ही प्रकार के सैनिक गुटों
से अलग रहने का निश्चय किया और किया कि वह किसी सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा, स्वतंत्र
विदेश नीति अपनाएंगा तथा प्रत्येक राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्न पर स्वतंत्र तथा
निष्पक्ष रूप से विचार करेगा।
(2) उपनिवेशवाद
व साम्राज्यवाद का विरोध :— संघर्ष
और युद्धों का सबसे बड़ा कारण साम्राज्यवाद है। भारत स्वंय साम्राज्यवादी शोषण का
शिकार रहा है द्वितीय महायुद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका व लैटिन
अमेरिका के अधिकांश राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। पर साम्राज्यवाद का अभी पूर्ण विनाश
नहीं हो पाया है। भारत ने एशियाई और अफ्रीकी देशों की एकता का स्वागत किया है।
(3) अन्य
देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध:—
भारत की विदेश नीति की अन्य विशेषता यह है कि भारत विश्व के अन्य
देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए सदैव तैयार रहता है।
(4) पंचशील
और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व :—
पंचशील का अर्थ है पांच सिद्धांत। यह सिद्धांत हमारी विदेश नीति के
मूल आधार है। इन पांच सिद्धांत के लिए पंचशील शब्द का प्रयोग सबसे पहले 24
अप्रैल, 1954 इसवी को किया गया था। यह सिद्धांत है कि यदि
इन पर विश्व के सब देश चले तो विश्व शांति स्थापित हो सकती है। यह पांच
सिद्धांत निम्नलिखित है:—
(1) एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसता को बनाए रखना।
(2) एक दूसरे पर आक्रमण ना करना।
(3) एक दूसरे के अंतरिक्ष मामलों में हस्तक्षेप ना करना।
(4) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत को मानना।
(5) आपस में समानता और मित्रता की भावना को बनाए रखना।
प्रशन 5:—राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा
उत्तर:
—भारत
प्रारम्भ से ही शांतिप्रिय देश रहा है इसलिए उसने अपनी विदेश नीति को राष्ट्रीय
हितों सिद्धांत पर आधारित किया है। इसी कारण आज भारत आर्थिक, राजनीतिक
हुआ संस्कृतिक क्षेत्रों में शीघ्रता से उन्नति कर रहा है। इसके साथ साथ वर्तमान
समय में भारत के संबंध विश्व की मां शक्तियों (रूस तथा अमेरिका) एवं अपने लगभग सभी
पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण और अच्छे हैं।
प्रशन 15:-- भारत पाक संबंधों पर संक्षिप्त लेख लिखे।
उत्तर:
—भारत
पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश हैं। पाक का जन्म 1947 में भारत से ही
हुआ था। किंतु प्रारंभ से ही इन दोनों के संबंध अच्छे नहीं रहे। कश्मीर को लेकर 1948
में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। 1965 तथा 1971
में भी भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए। इसके पश्चात शिमला समझौता हुआ जिसमें
दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ना केवल आशीर्वाद दिया बल्कि प्रशिक्षण
भी दिया है। आतंकवादियों की मार्फतपाकिस्तान में पंजाब और जम्मू कश्मीर में अशांति
का दौर पैदा किया और आम लोगों के जानमाल को भारी क्षति पहुंचाई। कश्मीर घाटी में
आतंक फैलाने की सारी योजनाएं पाक कब्जे वाले कश्मीर में बनती है और वह उन्हें सीमा
के इस पार लागू करवाता रहता है।
20 फरवरी, 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेई ने पाकिस्तान की बस
यात्रा की। बाघा चौकी को पार करने पर सीरी वाजपेई का भव्य स्वागत हुआ। यात्रा एक
ऐतिहासिक अद्वितीय घटना सिद्ध हुई। 21 फरवरी, 1999 को
भारत-पाक के बीच लाहौर समझौता हुआ। इसके अंतर्गत कश्मीर समेत सभी समस्याओं को
सुलझाने का प्रथम किया गया है। इस ऐतिहासिक कदम की अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान
सहित सारे विश्व में भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को दोनों देशों की जनता ने
हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने पाकिस्तान के साथ सहयोग
का एक मजबूत ढांचा खड़ा करने की कोशिश की पर शीघ्र ही उनका यह प्रयास उस समय धूल
में मिल गया जब मई 1999 में पाकिस्तान के सैनिको द्वारा कारगिल क्षेत्र में भारी घुसपैठ की
घटना घटी। भारत ने इसके खिलाफ ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया। र्मोच पर भारी पराजय
और अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा से पीछे हटना पड़ा।
प्रशन 16:— भारत रूस संबंध पर संक्षिप्त लेख लिखें
उत्तर:
—भारत
में साम्यवादी राज्य के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं ,लेकिन
भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण
पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है या रूस
संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साहित्य का इतिहास है।
रूस और भारत का बहु्धुवीय विश्व से आशय यह है कि अंतरराष्ट्रीय फलक
पर कई शक्तियां मौजूद हो, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो (यानी किसी
भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्यवाही
करें) 36 गांव को ज्यादा जगह मिले, अंतरराष्ट्रीय
संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो,हर देश की
स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाए
तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के
भारत रूस सामाजिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80
द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं।
भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा
आपूर्ति , अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान, पश्चिमी
एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मामलों
में फायदे हुए हैं। रूस को भारत के संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस
के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीददार देश है। भारतीय सेना को अधिकार सैनिक
साजो समान रूप से प्राप्त होते हैं क्योंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए
भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की
मदद की है। भारत रूस से अपनी उर्जा-आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
प्रशन 17:-- आपातकाल की घोषणा की क्या कारण थे?
उत्तर:--
1975 में लगाया गया
आपातकाल आवश्यक, उचित तथा वैध था नहीं इसके बारे में स्वाभाविक रूप से पक्ष और विपक्ष
में तर्क दिए गए थे। सरकार ने इसे आवश्यक तथा तुरंत उठाया जाने वाला कदम बताया था
क्योंकि यदि इसमें देर की जाती तो देश में बगावत हो सकती थी।
* सरकार का कहना था कि वह चुनाव के नतीजों के आधार पर बनी सरकार है, जनता
के आदेश के आधार पर अस्तित्व में आई है। उसे काम करने, अपनी
नीतियों को लागू करने, चुनाव में जनता से किए काए गए वायदों को पूरा
करने के लिए, योजनाओं को लागू करने का अवसर मिलना चाहिए। विपक्षी दलों को चाहिए की
निर्वाचित सरकार को काम करने दे, उसके रास्तों में बाधा ना डालें
* सरकार का यह भी कहना था कि हर रोज का धरना, हड़ताल, प्रदर्शन, विपक्षी
दलों की सामूहिक बाधाए राष्ट्र के दैनिक जीवन को बाधित करती है, जो
उचित नहीं है।
* यह भी कहा गया था कि विपक्षी दल लगातार गैर संसदिय राजनीति तथा देश
के लिए घातक गतिविधियों का सहारा सहारा ले रहे हैं और इसमें राजनैतिक अस्थिरता
पैदा होती है तथा देश की सामाजिक आर्थिक विकास प्रक्रिया बाधित होती है किसकी
सरकार को अपना ध्यान सबसे पहले कानून व्यवस्था को बनाए रखने पर लगाना पड़ता है उस
पर अनावश्यक खर्च बढ़ता है।
* भारतीय साम्यवादी दल जो सरकार के साथ थी का कहना था कि भारत के
विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय मंच पर साजिश की जा रही है और विपक्षी दल उसमें योग दे रहे
हैं। उसका इशारा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी पूंजीवादी देशों की ओर
था। साम्यवादी दल का कहना था कि जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे
हैं वह मध्यम वर्ग की क्रांति है, जनसाधारण की क्रांति नहीं, सर्वहारा
वर्ग की क्रांति नहीं।
प्रशन 18:—आपातकाल की घोषणा के प्रभाव पर प्रकाश डालें।
उत्तर:
—जून
1975 में भारत में आंतरिक कारणों से आपात काल का लगाया जाना भारतीय
राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि इस प्रकार जनता
द्वारा निर्वाचित एक लोकप्रिय सरकार भी प्रजातंत्र में अधिनायक वादी हो सकती है।
तमाम सरकारी नियंत्रणों के बावजूद आपातकालीन
तानाशाही का भारत की जनता तथा विपक्षी राजनीतिक दलों ने विरोध किया।
आपातकाल विरोधी आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने किया
उन्होंने नारा दिया, डरो नहीं अभी मैं जिंदा हूं’।आपातकाल के
विरोध के चलते विपक्षी दलों ने आपसी मतभेद भुलाकर जनता पार्टी नामक एक नई पार्टी
का गठन किया जिसमें संगठन कांग्रेश, जन संघ, समाजवादी
दल का विद्रोही कांग्रेसियों के गुट सम्मिलित थे।
मार्च 1977 में जो चुनाव संपन्न हुए उनका प्रमुख मुद्दा ‘लोकतंत्र
बनाम तानाशाही’था जिसमें लोकतंत्र के रूप में जनता पार्टी को विजय हासिल हुई तथा
तानाशाही के प्रतिक के रूप में कांग्रेश की हार हुई। इन चुनाव में यह सिद्ध कर
दिया कि यदि भारतीय राजनीति में विपक्ष में एकता स्थापित हो जाए तो वह कांग्रेश का
सशक्त विकल्प बन सकती है। 1977 में गठित जनता पार्टी की सरकार वस्तुत: केंद्र
में पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी।
सरकार की ज्यादित्यो के कारण सरकारी कर्मचारियों और मशीनरीयो मैं सक्रियता
आ गई। कुछ समय के लिए सौंपा गया अनुशासन दिखाई दिया लेकिन 18
मास के बाद संकटकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। विरोधी दलों और मतदाताओं ने
अपनी जितनी राजनीतिक जागृति दिखाई इससे साबित हो गया कि बड़े से बड़ा तानाशाही
नेता भी भारत से लोकतंत्र विदा नहीं कर सकता।
आपातकाल के बाद संविधान में अनेक सुधार किए गए। अब आपात काल सशर्त
स्थिति में ही लगाया जा सकता था। ऐसा तभी हो सकता था जब मंत्री मंडल लिखित रूप से
राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे।
आपातकाल में भी न्यायालयों मैं व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा
करने की भूमिका सक्रिय रहेगी और नागरिक अधिकारों की रक्षा तत्परता से होने लगी।
प्रशश 19:— भारतीय राजनीति पर क्षेत्रवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
या:—भारत में क्षेत्रीयता के दुष्परिणामों का उल्लेख करें।
उत्तर:—
क्षेत्रवाद
भारतीय राजनीति की एक प्रमुख विशेषता है। क्षेत्रवाद का तात्पर्य ऐसी चेतना से है
जिसमें क्षेत्रीय पहचान ही राजनीति प्रक्रिया में भागीदारी का प्रमुख आधार होती है
क्षेत्रीय पहचान, विशिष्ट संस्कृति, भाषा, भौगोलिक
परिस्थिति या प्रजाति के आधार पर विकसित हो सकती है। भारत में इस तरह की क्षेत्रीय
विभिन्नताएं सदैव विद्यमान रही है। राजनीति में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति , क्षेत्रीय
दलों का निर्माण, क्षत्रिय आंदोलनों का विकास अथवा अलगाववाद के रूप में देखी जा सकती
है संपर्क में भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद का प्रभाव निम्न रूपों में दिखाई
देता है—
(1) क्षेत्रवाद का उग्र वा हिंसात्मक रूप राष्ट्रीय
एकता व अखंडता के लिए खतरा है। उदाहरण के लिए कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन, पंजाब
में खालिस्तान की मांग अथवा पूर्वांतर राज्य में अलगाववाद की प्रवृतियां इसी तरह
के खतरे हैं।
(2)क्षेत्रवाद अपने सामान्य रूप में क्षेत्रीय तथा
अथवा अलग राज्य की मांग का रूप ले सकता है। 1956 में भाषा के
आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। उत्तराखंड झारखंड व छत्तीसगढ़ का
निर्माण इसी आधार पर हुआ है। वर्तमान में बुंदेलखंड, तेलंगाना व
गोरखालैंड (दार्जिलिंग) मैं अलग राज्यों की मांग इसके प्रमुख उदाहरण है
(3) छत्तीसगढ़ लोक की अधिक मजबूती के कारण राजनीतिक
अस्थिरता उत्पन्न होती है। वर्तमान में केंद्र में गठबंधन सरकारों का निर्माण
क्षेत्रवाद का परिणाम है।
(4) चक्रवात के कारण राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे गौण
हो जाते हैं तथा क्षेत्रीय हित राष्ट्रीय हितों पर हावी हो जाते हैं।
(5) क्षेत्रवाद का एक सकारात्मक प्रभाव यह है कि
इससे क्षेत्रीय समस्याओं को राजनीति में समुचित ज्ञान प्राप्त हो जाता है तथा
अत्यधिक केंद्रीय करण की प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है। संघात्मक व्यवस्था की दृष्टि
से इसे उचित माना जा सकता है।
ये भी पढ़े ...
Class 12th Political Science :- Click Here
Class 12th History :- Click Here


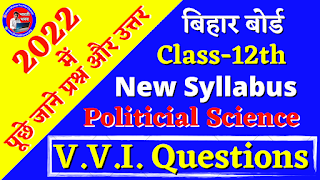
Hello My Dear, ये पोस्ट आपको कैसा लगा कृपया अवश्य बताइए और साथ में आपको क्या चाहिए वो बताइए ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ धन्यवाद |